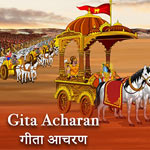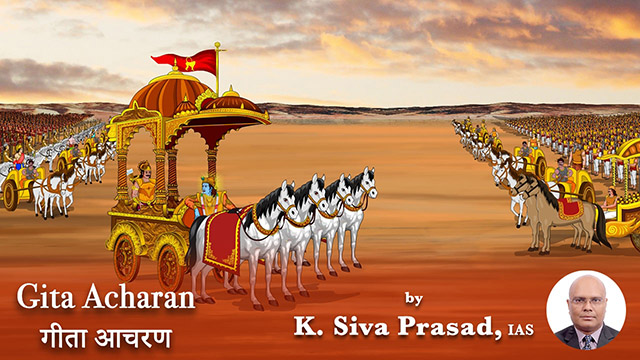
जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। यह निर्भर करता है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तो वह निराश हो जाता है और कर्मों को त्यागने की ओर उन्मुख हो जाता है, क्योंकि हम सभी इस भ्रम में हैं कि हमारे कर्म के साथ-साथ दूसरों के कर्म भी हमें सुख या दु:ख देते हैं। अर्जुन भी इसी भ्रम से गुजर रहे हैं और युद्ध लडऩे का कर्म छोडऩा चाहते हैं।
श्रीकृष्ण स्पष्ट करते हैं कि, ‘‘जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह संन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला संन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है’’ (6.1)।
करने योग्य कर्म के संबंध में जितना स्पष्टीकरण दिया जाए उतना ही ज्यादा संशय पैदा कर सकता है क्योंकि यह विशुद्ध रूप से अनुभवात्मक है। तैरना सीखने के लिए व्यक्ति को पानी मे गोते लगाने पड़ते हैं और ठीक इसी तरह करने योग्य कर्म को समझने के लिए जीवन का अनुभव करना होगा। इन्द्रियों की सहायता के बगैर खुश रहना हमारी प्रगति को मापने का वैसा ही मानदंड है जैसे तैरने के लिए तैरना।
इसी तरह एक बीजकोष से अपेक्षा की जाती है कि वह भ्रूण की रक्षा करे और साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि सही परिस्थितियों में अंकुरित होने का रास्ता भी दे। हालांकि यह हमें स्वाभाविक लगता है, बीजकोष के दृष्टिकोण से यह भ्रमित करने वाला है कि एक बार संरक्षण करना और बाद में नहीं करना। बीजकोष के मामले की तरह, सर्वशक्तिशाली वर्तमान क्षण द्वारा हमें प्रदान किए गए कर्म को अतीत के बोझ और भविष्य की अपेक्षाओं के बिना करना ही करने योग्य कर्म है।
दूसरा, श्रीकृष्ण कहते हैं कि संन्यासी वह है जो कर्मफल छोड़ देता है लेकिन कर्म नहीं छोड़ता। यह उस आत्म-तृप्ति के लिए प्रचलित कथन को नकारता है जिसमें कहा गया है कि ‘कर्म न करने का अर्थ है न दु:ख और न पाप’। श्रीकृष्ण का मार्गदर्शन हममें से प्रत्येक को पलायनवाद का सहारा लिए बिना संन्यासी बनने के योग्य बनाता है। परिस्थितियाँ जैसी भी हों, जिस क्षण कोई कर्मफल की आशा छोड़ देता है, उसी क्षण वह संन्यासी के आनंद को प्राप्त करता है।