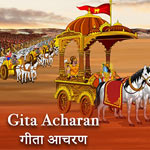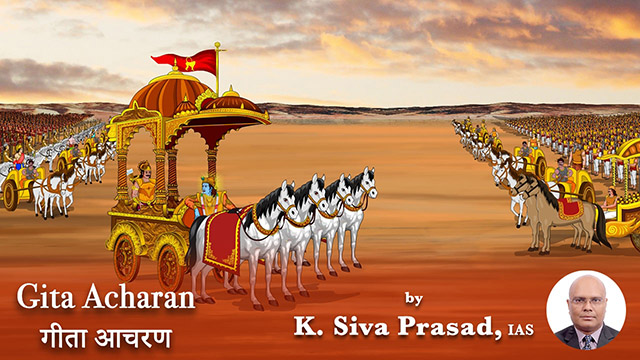
अज्ञान के कारण व्यक्ति भौतिक संपत्ति को हड़पने में लगा रहता है जिससे कर्मबंधन में बंधता है। जब जागरूकता की पहली किरण उतरती है, तो वह त्याग के बारे में सोचने लगता है जैसे अर्जुन यहां कोशिश कर रहे हैं। भ्रम इस बात में है कि क्या त्याग करें। सामान्य प्रवृत्ति सभी कर्मों या कार्यों को त्याग करने की होती है, क्योंकि हम उन्हें हमेशा अपने विभाजन करने वाले मन से अच्छे या बुरे के रूप में विभाजन करते हैं और अवांछित कर्मों को छोडऩा चाहते हैं।
दूसरी ओर, श्रीकृष्ण त्याग के संबंध में एक अलग धारणा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ‘‘जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी नित्यसंन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग-द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारबंधन से मुक्त हो जाता है’’ (5.3)। पहली चीज जिसका हमें त्याग करना चाहिए वह है द्वेष। यह किसी भी चीज के प्रति हो सकता है जो हमारी मान्यताओं के खिलाफ जाती है जैसे धर्म, जाति या राष्ट्रीयता। नफरत हमारे पेशे, लोगों या हमारे आसपास की चीजों के प्रति हो सकती है। अंतर्विरोधों में एकता देखना महत्वपूर्ण है। नित्य संन्यासी द्वेष के साथ-साथ इच्छाओं का भी त्याग करता है।
श्रीकृष्ण हमें द्वेष और इच्छाओं जैसी प्रवृत्तियों को त्यागने का परामर्श देते हैं। सच्चाई यह है कि कर्मों का कोई वास्तविक त्याग नहीं है क्योंकि हम एक कर्म का त्यागकर अपने गुणों के प्रभाव में दूसरे कर्म को करने लगते हैं। इसलिए हमें अपने बाहरी कर्मों के बजाय हमारे अंदर रहने वाले विभाजन को त्यागना चाहिए।
श्रीकृष्ण आगे कहते हैं, ‘‘ज्ञानयोगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है।
इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फलरूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है’’ (5.5)। कर्मयोग के बिना होने वाले अर्थात् मन, इन्द्रिय और शरीर द्वारा होने वाले सम्पूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवान स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है’’ (5.6)।
कर्म वह यंत्र है जो हमें यह पता लगाने में मदद करते हैं कि हम कितनी घृणा या इच्छाओं से भरे हुए हैं। इसलिए, श्रीकृष्ण कर्मों को त्यागने के बजाय निष्काम कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।