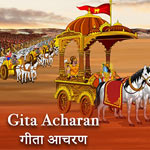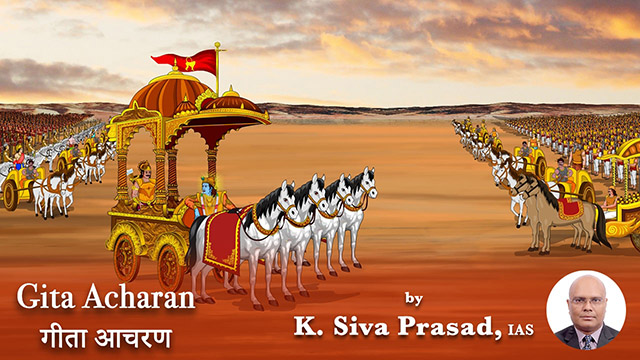
‘मन में आग’ होने का अर्थ है भौतिक दुनिया में अपनी इच्छाओं, रुचियों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा होना। जब ऐसी ऊर्जा का उपयोग आत्म-साक्षात्कार के लिए किया जाता है तो इसे योग-अग्नि कहा जाता है। इस सन्दर्भ में, श्रीकृष्ण कहते हैं कि, ‘‘दूसरे योगीजन इन्द्रियों की सम्पूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योगरूप अग्नि में हवन किया करते हैं’’ (4.27)।
दैनिक जीवन में हम परमात्मा को सुंदर फूल और स्वादिष्ट भोजन जैसी इंद्रिय वस्तुएं चढ़ाते हैं। यह श्लोक हमें इससे परे ले जाता है और कहता है कि यज्ञ स्वाद, सौंदर्य या गंध जैसी इंद्रिय गतिविधियों का चढ़ावा देना है, न कि केवल इंद्रिय वस्तु। इन्द्रियाँ विषयों के प्रति आसक्ति के द्वारा हमें बाह्य जगत से जोड़ती रहती हैं और जब इन इन्द्रियों की बलि दी जाती है, तो विभाजन समाप्त हो जाता है व एकता प्राप्त हो जाती है।
श्रीकृष्ण आगे कहते हैं, ‘‘कई पुरुष द्रव्य संबन्धी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं’’ (4.28)।
श्रीकृष्ण ने यज्ञ में से एक के रूप में स्वाध्याय का उल्लेख किया। इस प्रक्रिया ने मनोविज्ञान, चिकित्सा और समकालीन स्वयं सहायता रचना जैसे कई विषयों को जन्म दिया। बचपन से ही हमें जन्म के समय अर्जित कारकों जैसे कि राष्ट्रीयता, जाति या धर्म पर वर्गीकृत किया जाता है। हम अपना शेष जीवन इन विभाजनों का बचाव करने में व्यतीत करते हैं। कम उम्र में ही बहुत अधिक दमन या हिंसा के कारण वर्गीकरण का भाव हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसी प्रकार बुद्धिमान या बुद्धू, मेहनती या आलसी जैसी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण होता है और इनका अंत नहीं है।
इसी तरह, हम कई कारकों के आधार पर अपने और दूसरों के बारे में धारणा बनाते हैं और उसी के पक्ष में ऊर्जा खर्च करते हैं। स्वाध्याय इन विभाजनों का यज्ञ के रूप में परीक्षण करना और उनका त्याग करना है।