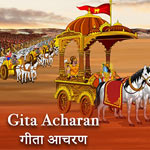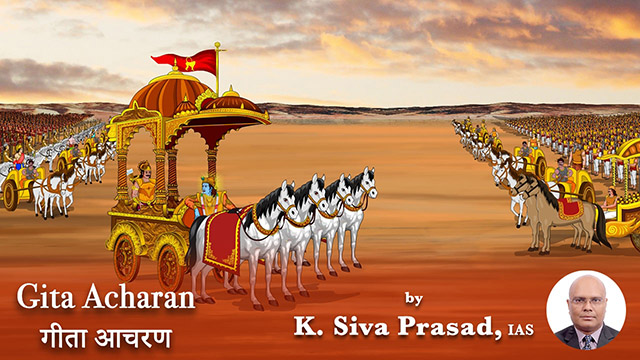
विकर्म (निषिद्ध कर्म) या पाप का प्रश्न बहुत जटिल है। अर्जुन भी इसी दुविधा में है और कहता है कि युद्ध में संबंधियों को मारने से पाप ही लगेगा (1.36)। वास्तव में, संस्कृतियों ने विभिन्न कर्मों को पापों के रूप में परिभाषित किया है और यह सूची समय के साथ बदलती रहती है। आधुनिक युग में, देशों के अपने पीनल कोड यानी दंड संहिता होती हैं जो कुछ कार्यों को अपराध या पाप मानती हैं। दंडसंहिता के अनुरूप व्यवहार न करने पर दंडनीय होते हैं। जब हमारे द्वारा ऐसे कथित पाप हो जाते हैं, तो हम खुद को ही अपराधबोध, अफसोस और शर्म की सजा लम्बे समय तक देते रहते हैं।
इस सन्दर्भ में, श्रीकृष्ण कहते हैं कि, ‘‘आशारहित, नियंत्रित मन और शरीर के साथ, सभी संपत्ति को त्याग कर, केवल शारीरिक कार्य करने वाला, कोई पाप नहीं करता’’ (4.21)। श्रीकृष्ण ने पहले पाप के बारे में बात की और अर्जुन से कहा, सुख और दु:ख; लाभ और हानि; जीत और हार को समान रूप से मानो और युद्ध करो, जिससे उसे कोई पाप नहीं होगा (2.38)।
पाप का मूल्यांकन करने में समझने वाली सूक्ष्म बात यह है कि हम आमतौर पर भौतिक दुनिया में अपने द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं, जबकि श्रीकृष्ण के लिए यह आंतरिक घटना है। हम से जो कर्म होता है वह हमारे मन की स्थिति का परिणाम है और श्रीकृष्ण हमें मन के स्तर पर नियंत्रण करने के लिए कहते हैं। दार्शनिक स्तर पर, यह हमारे अंदर कई शंकाएं पैदा करता है, लेकिन अनुभवात्मक स्तर पर, व्यक्ति स्पष्टता प्राप्त करता है।
श्रीकृष्ण आगे कहते हैं कि, ‘‘जो बिना इच्छा के अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईष्र्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है- ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता’’ (4.22)। वस्तुत: इस श्लोक को गीता का सूक्ष्म रूप कहा जा सकता है जिसमें विभिन्न स्थानों पर गीता में दिए गए सभी उपदेश समाहित हैं।
श्रीकृष्ण हमें द्वंद्वातीत होने के लिये कहते हैं। इसका मतलब विभाजनकारी मन का उपयोग केवल शारीरिक कार्यों के लिए करने के अलावा और कुछ भी नहीं।