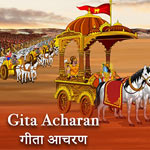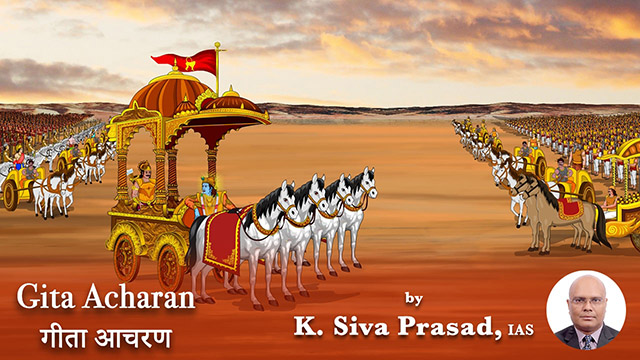
दैनिक जीवन में हम अपनी पसंद के कुछ कर्मों से जुड़ जाते हैं। इसे आसक्ति कहते हैं। हम कुछ कर्मों से नफरत की वजह से अलग हो जाते जिसे विरक्ति कहा जाता है। परन्तु श्री कृष्ण एक तीसरी अवस्था का उल्लेख करते हैं, जिसे अनासक्ति कहते हैं। यह आसक्ति और विरक्ति को पार करना है। उनका कहना है ( 3.25 ) कि आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, एक अनासक्त विद्वान भी लोकसंग्रह करने की चाह रखने के बावजूद उसी प्रकार कर्म करे।
आसक्ति और विरक्ति पर आधारित कर्म हमें दुखी कर सकते हैं। किसी प्रियजन (आसक्ति) की उपस्थिति हमें खुशी देती है और उनकी अनुपस्थिति हमें दुखी करती है। इसी प्रकार, घृणा करने वाले ( विरक्ति) की उपस्थिति हमें दुखी करती है और | उनकी अनुपस्थिति से राहत मिलती है। इसलिए आसक्ति या विरक्ति दोनों हमें सुख और दुख के ध्रुवों के बीच झुलाने में सक्षम हैं। तभी श्री कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि किसी भी कार्य को करते समय, दोनों को पार कर अनासक्त बनें।
संसार के कल्याण को करुणा के समान समझा जा सकता है जो अनासक्ति के साथ कर्म करने पर उभरकर आती है। जब कर्म आसक्ति या विरक्ति के साथ किया जाता है, तो यह एक कचरा ट्रक की तरह है जो हर जगह गंदगी फैलाता है, जिसका मतलब समाज को हानि पहुंचाना है।
अनासक्त किसी नाटक में अभिनय करने के साथ ही दर्शक बन कर उसकाआनंद लेने जैसा है। अभिनेता से की जाती है कि वह उसे दी गई भूमिका को समर्पण और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ पेश करे।
इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संबंधित कार्य क्षेत्र में अपने कौशल, ज्ञान आदि को बढ़ाते रहना चाहिए और साथ ही नाटक देखने वाले दर्शकों का हिस्सा भी होना चाहिए। यहां अभिनेता बाहरी दुनिया में हमारे कर्त्तव्य के समान है जबकि दर्शक हमारा आंतरिक रूप है।
सभी क्रियाओं को करते समय अनासक्ति का अभ्यास किया जाना चाहिए । जब हम इस प्रक्रिया में महारत हासिल कर लें तो समझ लें कि गीता कार्यान्वित हो गई है।